डा० रमा शंकर शुक्ल
हिंदी साहित्य का अतीत देखें तो दो काल-खण्डों के अलावा कविता कभी राष्ट्र्धर्मी नहीं रही. या यूं कहें की साहित्य ही राष्ट्र्धर्मी नहीं रहा. रीतिकाल में वीर रसात्मक कवियों के बाद आधुनिक काल के कवियों ने कविता को क्रान्ति का सहधर्मी बताया. लेकिन आधुनिक काल में प्रगतिवाद के बाद कविता ने नई दिशा ग्रहण कर ली. क्रान्ति की अवधारण राष्ट्रवादी के बजाय जनवादी हो गया. अर्थात कवी के मुकाबले में विदेशी आक्रान्ता नहीं स्वदेशी शातिर नव अधिनायकवादी अंग्रेज खड़े हो गए. प्रयोगवाद के बाद तो समूची कविता या फिर समूचा साहित्य ही घर की व्यवस्थाओं में बजबजा रही अव्यवस्था के विरोध स्वरुप लिखा जाने लगा. ऐसा नहीं है कि लेखकीय संघर्ष के केंद्र में राष्ट्र नहीं है, बल्कि उस संघर्ष का केंद्र अपनों की कुटिलता हो गई. परिणाम आपस में कांव-कांव का खडा हो गया. यह कांव-कांव अब भी जारी है साहित्यकारों ने इसी कांव-कांव को अपने लेखन का केंद्र-बिंदु मान लिया है. संभवतः यही कारण है कि दर्प के इन मतभेदों को निरुपित करने के लिए आज की तारीख प्रकाशित होने वाली हिंदी पत्रिकाओं की भरमार है, पर उसमे राष्ट्र नहीं है.
आधुनिक काल के तीन चरणों और समकालीन चरणों में यदि तुलनात्मक फर्क करें तो एक बात साफ़-साफ़ नजर आती है. पहले रचनाकार क्रांतिकारी भी होता था. वह लिखता था और उसे अमल में लाने के लिए किसी और के कंधे की बजाय खुद का कंधा इस्तेमाल करता था. आज का साहित्यकार चेतना का आत्ममुग्ध ठेकेदार है. उसने संघर्ष और चिंतन की विभाजक रेखा खींच दी है. वह मानता है कि उसे केवल सोचने का काम करना चाहिए. जूझने वाला वर्ग कोई दूसरा हो. अर्थात, वे खुद को पैदाइसी नियामक मान रहे हैं. नियामक कभी स्वयं युद्ध नहीं करता. उदाहरण के तौर पर राम मंदिर निर्माण आन्दोलन को लिया जा सकता है. बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद् और उमा भारती-विनय कटियार सरीखे भाजपा नेता अपने बयानों में शहीदी मुद्रा में कहते हैं कि हम हजारों कारसेवकों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे. लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता कि हजारों कारसेवकों के तरह मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवानी, अटल बिहारी वाजपेयी, कटियार, उमा भारती आदि लोगों ने शहीद होने का जज्बा क्यों नहीं दिखाया? तो शायद कही न कहीं इनमे खुद के नियामक होने की ग्रंथि रही कि हमें केवल नेतृत्व करने का अधिकार है, जूझने और मरने के लिए दूसरे लोग बने हैं.
जहाँ तक मै जानता हूँ कि सरदार पूर्ण सिंह ने महज पांच निबंध लिखे थे, जिसके आधार पर वे हिंदी साहित्य में अमर हो गए. नरोत्तम दास ने भी सुदामा चरित मात्र लिखा और अमर हो गए. आज हमारे अनंत साहित्यकार नियामक कई दर्जन पुस्तकों के मालिक हैं. वे गणनात्मक उपलब्धियों में क्रांतिकारी कवियों और साहित्यकारों से बहुत ज्यादा लिख चुके हैं, लेकिन जनता उन्हें अपना कवि नहीं मान रही. जबकि हरिओम पवार और कुमार विश्वास सरीखे लोग जनकवि की भूमिका में खड़े हैं. लोग उन्हें सुनना चाहते हैं. वे उन्हें गुनगुना रहे हैं. दुष्यंत कुमार आज भी लोगों की जुबान पर हैं. निराला जनता के ज्यादा करीब हैं. धूमिल ज्यादा करीब हैं. क्यों? इसलिए कि लोग देख रहे हैं कि ये फर्जी नहीं कह रहे हैं. बल्कि खुद जूझ रहे हैं. निराला और धूमिल ने भी संघर्ष किया. नामवर सिंह समेत अनेक नामवर लोग इस जनता के कहाँ करीब हैं?
सच तो यह है कि आज कवियों/साहित्यकारों की भरमार है. हर मोहल्ले में कोई न कोई कवि है. साहित्यकार है. लेकिन उसे मोहल्ले के लोग ही नहीं जानते. उनका किसी पर कोई प्रभाव नहीं है. क्यों? इसका उत्तर एक दूसरे क्षेत्र के उदाहरण से समझा जा सकता है. भारत में इस समय हिन्दू धर्म में लाखों सन्यासी, मथाधीस, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, बापू आदि लगातार आचरण सुधार का प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन भक्तों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है. इसलिए कि प्रवचन करने वाले का आचरण उनके उपदेशों के विपरीत है. अब भला कोई व्यक्ति किसी सन्यासी अथवा शंकराचार्य को भौतिक वस्तुओं के सभी प्रकार के सुख का भोगना देख रहा हो और पाई-पाई का हिसाब रख रहा हो. दर्जनों-सैकड़ों आलिशान मठ, आलिशान गाड़ियाँ लिए घूम रहा हो तो भला उसके द्वारा भूंके गए उपदेश कैसे असर करेंगे. एना हजारे के साथ अगर देश के करोड़ों लोग खड़े हो गए, अरविन्द केजरीवाल के साथ खड़े हो रहे हैं तो सीधा कारण है कि उनके आचरण में राष्ट्रीयता झलक रही है. महसूस कर रहे हैं कि ये केवल बोल नहीं रहे, बल्कि राष्ट्र को जी भी रहे हैं. वे साधना कर रहे हैं. वे इतना तप रहे हैं कि थोडा सा भी लिजलिजा व्यक्ति सामने जाए तो वह भी तपने लगेगा. जबकि धर्म हमारे जीवन का सबसे प्रभावशाली तत्व होने के बाद भी हमारे संतों को अपनी बात कहने के लिए लाखों खर्च कर प्रवचन स्थल का निर्माण करना पड़ता है.
कुछ इसी मुद्रा में समकालीन साहित्य भी है और साहित्यकार भी हैं. वे साहित्यकार कम शब्दों के खिलाड़ी ज्यादा हैं. वे भाषा के मदारी हैं. मदारी का करतब मनोरंजन के लिए होता है न कि निर्माण के लिए. अब आज की तारीख में साहित्य क्रान्ति नहीं कर रही है. हैरत होती हैं जब युवा से युवा कवि भी अपनी कविता निजी प्रेम संबंधों, असफलताओं, हताशाओं की अभिव्यक्ति के रूप में रचता है. हमारे वर्त्तमान कथित कतिपय स्वयंभू मनीषी कहते हैं कि यह नव उदारीकरण का प्रभाव है. साहित्य समाज का दर्पण ही तो है. युग का निरूपण ही तो साहित्य है.......... वगैरह-वगैरह. तो फिर समाज को जगाने वाला कौन होगा. वह कहाँ से आयात होगा! क्या साहित्यकार जन-मन का निर्माण नहीं करता? नवीन, मैथिलीशरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर जैसे राष्ट्रीय चेतना के कवि युगधर्मी नहीं थे? लेकिन उन्होंने जन-मन को जगाया. जगाने का प्रभाव सामने है. आजादी के लड़ाई में कविता और साहित्य भी किसी हथियार से कम नहीं था. बल्कि यह सबसे बड़ा हथियार था. दुःख है कि कविता से वह आग निकल चुकी है. वह शोर में गम हो जा रही है. इसलिए कि उसकी आवाज में वह नाद नहीं है. वह गर्जन नहीं है. चुभन नहीं है. जबकि परिस्थितियां अंग्रेजी गुलामी से ज्यादा भयावह और अनंत आशंकाओं की और संकेत कर रही हैं.
डा० रमा शंकर शुक्ल
Powered by Froala Editor



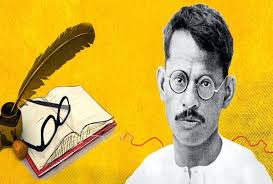
LEAVE A REPLY